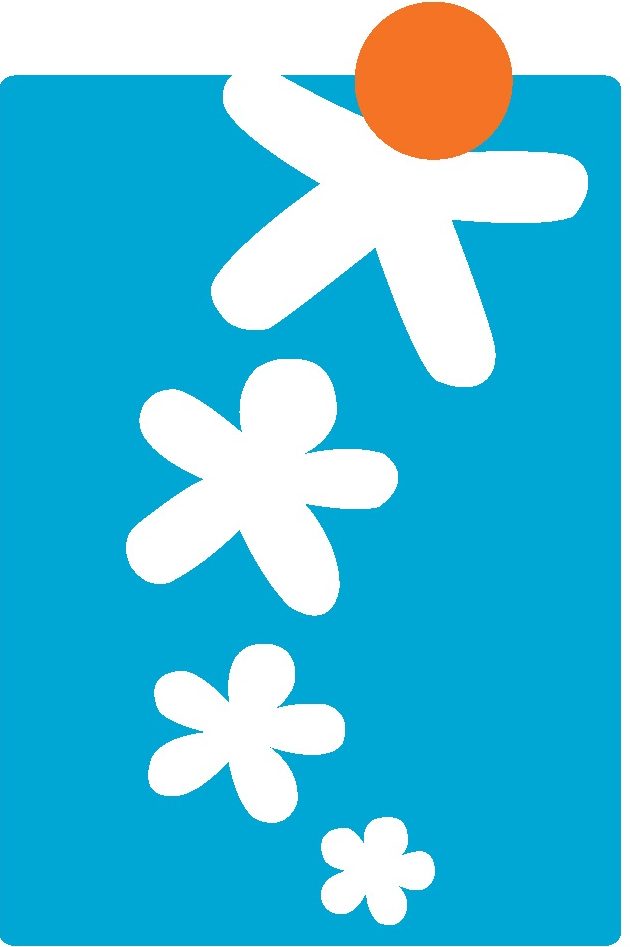रमेश दवे के द्वारा लिखी गई किताब मैं इस तरह नहीं पढूंगी, ग्रन्थ शिल्पी (इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली से २००४ में प्रकाशित हुआ | रमेश दवे एक शिक्षाशास्त्री हैं और लम्बे समय तक मध्य प्रदेश के शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर काम किया है| लेखक ने इस किताब को एक बच्ची के साथ वार्तालाप के स्वरुप में लिखा है |
एक बच्ची के मन में उठते सवालों के जवाब देते हुए लेखक ने बड़े ही सरल भाषा में शिक्षा के अनेक गूढ़ संकल्पनाओ एवं नवाचारों को सामने रखा है | पूरी किताब मुझे दो हिस्सों में प्रतीत होती है | एक हिस्से में शिक्षा के नवाचारों की बात है तो दूसरे हिस्से में व्यवस्था पर गहरी चोट दिखाती है | पूरी पुस्तक छोटे छोटे ३९ अध्यायों में बटी है | लेखन शैली की वजह से अगला अध्याय पिछले अध्याय से जुड़ा भी रहता है |
पुस्तक के शुरुआत मे बच्ची के द्वारा, स्कूल में भय से सम्बंधित चर्चा की गयी है | स्कूल आने की घंटी डराती है, क्यूंकि घंटी सुनते ही भागकर आना होता है | अगर समय पर न आये तो बाहर खड़ा कर देते है | प्रार्थना से डर, हाथ जोड़कर खड़ा कर देते हैं कतार में | हाजिरी का डर, टीचर चीख चीख कर ऐसे नाम बुलाते हैं जैसे थाने पर कोई सिपाही किसी अपराधी को बुलाता है | और ऐसे ही ढेरों डर जिसके वजह से बच्चे स्कूल आने से कतराते हैं | किसी भी इन्सान में व्याप्त तात्कालिक डर उसकी सीखने की प्रक्रिया को बाधित कर देता है और बच्चे इसका अपवाद नहीं हैं खासकर ऐसी जगह जहाँ वो अधिकारिक रूप से कुछ सीखने आते हैं |
आगे बढ़ने पर यह किताब बताती है की बच्चों की किताब कैसी होनी चाहिए | बच्चों की किताब बनाते वक़्त एक सूचि रखनी होगी कि बच्चों को क्या अच्छा लगता है और क्या नहीं | यह उनसे स्वयं, उनके माता पिता और शिक्षकों से मिलकर तय करना होगा | बच्चों के लिए भाषा, गणित, पर्यावरण, विज्ञान, और खेल कुछ अलग नहीं होता | उनके लिए यह सब एक ही है | इसलिए इनकी एक ही पुस्तक क्यूँ न हो जिनसे बच्चों को खेल की भाषा, खेल का गणित और खेल का पर्यावरण और विज्ञान मिले | हर किताब के पहले दो चार पन्ने खाली छोड़कर बच्चों के खेल के लिए जगह क्यों नहीं बनाई जा सकती ?
किताब बताती है की किस तरह बच्चे अपना पाठ्यक्रम खुद बना सकते हैं | अगर हम उनकी बातों का समावेश पाठ्यक्रम में करें तब भी बहुत हद तक बात बन जाती है|इसको सुंदर तरीके से बच्चों ने यह बताया कि: खेल को पाठ्यक्रम में सबसे पहले रखो | दुसरे नंबर पर प्रेम रखो | तीसरे नंबर पर मदद रखो | चौथे नंबर पर समाज रखो | इस तरह गीत, कविता, कहानी, खेल, नाटक, पहेली, और न जाने क्या क्या जादू बच्चों ने बताये | गणित का तो एक पिटारा ही खोल दिया | प्रेम का गणित, सहयोग का गणित, काम का गणित, खेल का गणित |
किताबी कीड़ा या किताबी क्रीडा: अगर बच्चों की किताब खेल, चुटकुलों, पहेलियों, कहानियों और गीतों से शुरू हों और हर पाठ के साथ बच्चों को कुछ न कुछ क्रिया करने को मिले तो बच्चे ऐसी किताब बार बार पढ़ेंगे| जब बच्चे खिलौनों की तरह ही किताब से भी खेलेंगे तब हमे उन्हें किताबी कीड़ा नहीं बनाना पडेगा अपितु वो सब किताबों से क्रीड़ा करते हुए सीखेंगे |
पुस्तक का दूसरा हिस्सा शिक्षा जगत के तंत्र पर चोट करती है | स्कूल को हमने कई तरह के डरों से लाद रखा है | लेकिन व्यवस्था का खौफ इस कदर है कि शिक्षक रात – दिन उसी डर में जीतें हैं | तरह तरह के पर्यवरेक्षक, निरीक्षक, आकलनकर्ता, ब्लाक, जिला और संभाग अधिकारी , पंचायत कर्मी , नेता और सरकारी, गैरसरकारी कई तरह के अमले स्कूल में इस तरह हस्तक्षेप करते हैं मानो स्कूल न हो कर सार्वजनिक सनक की जगह हो| खौफ उसके पक्ष को न समझते हुए, लगातार उसे जिम्मेदार ठहराने का, खौफ उसके ऊपर भरोसा ना करने का|
स्कूल के लिए बाल मनोविज्ञान है , क्या बाल मनोविज्ञान केवल बच्चों और शिक्षकों के लिये है ? उन माता पिता और ऐसे अपराधी किस्म के अफसरों को क्यों यह मनोविज्ञान नहीं सिखाया जाता की आजाद देश में वो जनता के सेवक हैं मालिक नहीं |
इस देश में प्रेम केवल सिनेमा के परदे पर ही बड़े रोमांटिक ढंग से दिखाया जाता है बाकी प्रेम की कमी इस कदर आ गयी है कि परिवारों की जीवनशैली में प्रेम भी एक वस्तु की तरह रह गया है| बच्चे संसाधन हो गए है |अगर प्रेम की शिक्षा होती तो लोग नफरत के दंगे नहीं करते, अपने ही देश की रेल, मोटर, स्टेशन नहीं जलाते, तोड़ फोड नहीं करते | जो देश अपने मनुष्यों, अपनी चीजों से, अपने काम से प्रेम करता है वह जल्दी तरक्की करता है |
आखिर क्या बात है की शिक्षा से कोई क्रांति आज तक नहीं हुई | जेल के कैदियों तक ने क्रांति की है मगर शिक्षा के मदरसों – कालेजों से शिक्षकों या छात्रों की तमाम राजनीती के बावजूद कोई क्रांति आज तक नहीं हुयी | कुछ अपवाद हो सकते हैं मगर एक सार्वभौम सत्य है कि कोई भी शिक्षा संस्था यह कायम नहीं कर सकी कि उसकी शिक्षा ने कोई क्रांति कर दी|
स्कूल को घर बनाइये, स्कूल को खेल बनाइये, स्कूल को पहेली बनाइये, स्कूल को जिज्ञासा, प्रश्न और खोज बनाइये, तब स्कूल बच्चों का आनंद बनेगा | स्कूल को त्यौहार और उत्सव बनाइये, नाटक, नौटंकी, तरह तरह के स्वांग लोकमंच में बदलिए, स्कूल से लोक जुड़ेगा, और स्कूल और लोक जब एक साथ होगा तब स्कूल से जो नया लोकरंग उपजेगा वह ख़ुशी और ख्वाहिश का लोकरंग होगा और खौफ का अँधेरा छटेगा |
जो स्कूल खेल पैदा करता है, वहां डर नहीं होता | खेल से मतलब केवल मैदान में खेला जाने वाले खेल ही नहीं अपितु कक्षा कक्ष में हो रही गतिविधिया इतनी रोचक हो की बच्चे उसमे वैसे ही प्रतिभाग करने की लिए आतुर हो जैसे की वह खेलने के लिए होते हैं और नियम हर खेल में होते है उन नियमों के साथ खेलना; जो स्कूल संगीत की मधुर ध्वनि पैदा करता है, वहां शोर नहीं होता; जो स्कूल कहानी पैदा करता है, वहां भाषणों की ऊब नहीं पैदा होती; जो स्कूल खोज और जिज्ञासा पैदा करता है वहां कोई हुनर छुपा नहीं रह सकता | जो स्कूल स्वावलंबन देता है उस देश में स्वाभिमान अपने आप आता है | जो ख़ुशी देता है , वहां कभी खौफ नहीं हो सकता|
अंत में स्कूल स्वयं अपनी बात कहता है कि मेरे दर्द की दास्ताँ बहुत लम्बी है | क्या क्या सुनाऊँ | अगर समाज और सरकार मुझे कमजोर बनाये रखना चाहतें हैं, मैं आपको ताकतवर बच्चे कैसे दूं ? अगर मेरी ही हड्डियों में जान नहीं तो मैं एक व्यायामशाला का रोल अदा कैसे करू? अगर मेरे ही अंदर से आनंद के झरने नहीं फूटते, तो में बच्चों को वो आनंद कैसे दूं जिसकी मांग सारे शिक्षाविद मुझसे करते हैं? अगर मेरी ही आँखों में आंसू हैं तो में बच्चों के आंसू कैसे पोंछूं ?
रमेश दवे (२००४). मैं इस तरह नहीं पढूंगी . दिल्ली: ग्रन्थ शिल्पी (इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड.